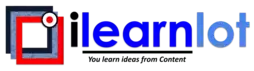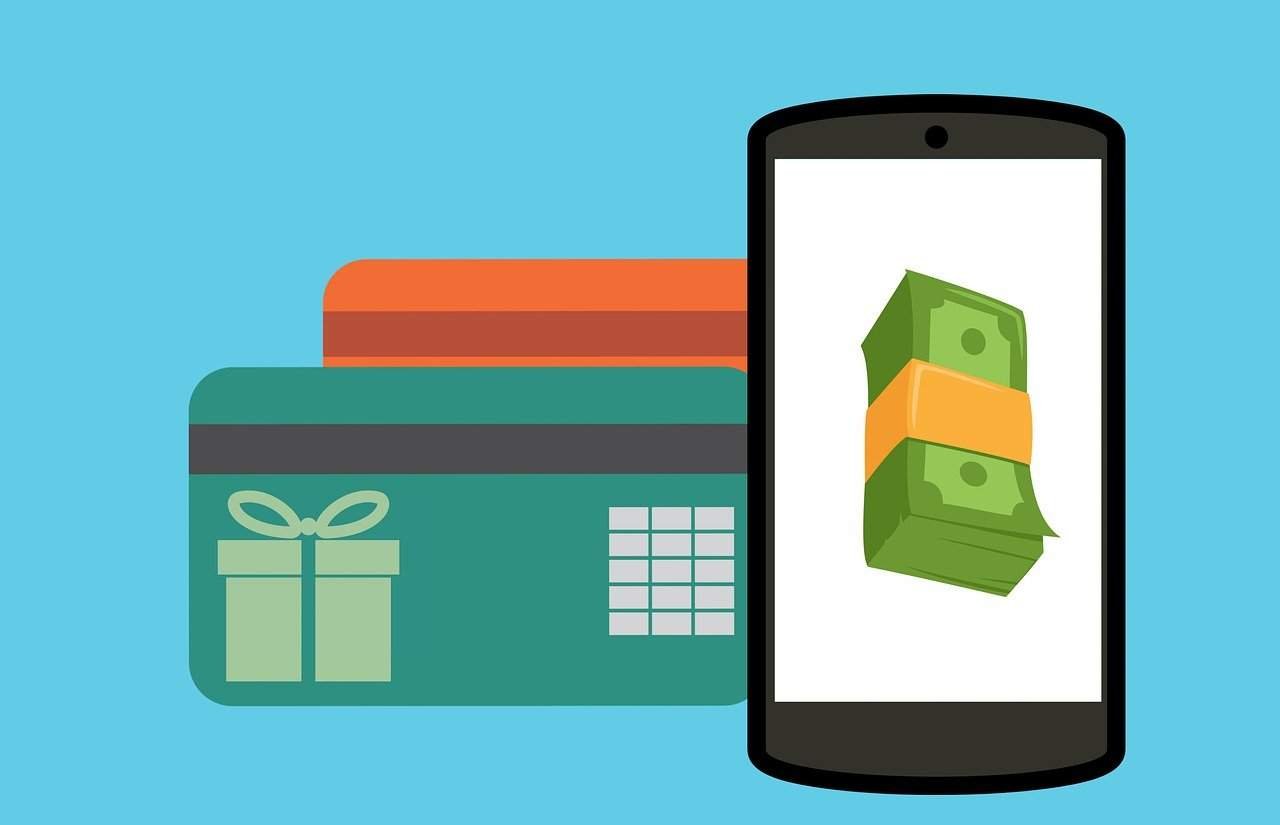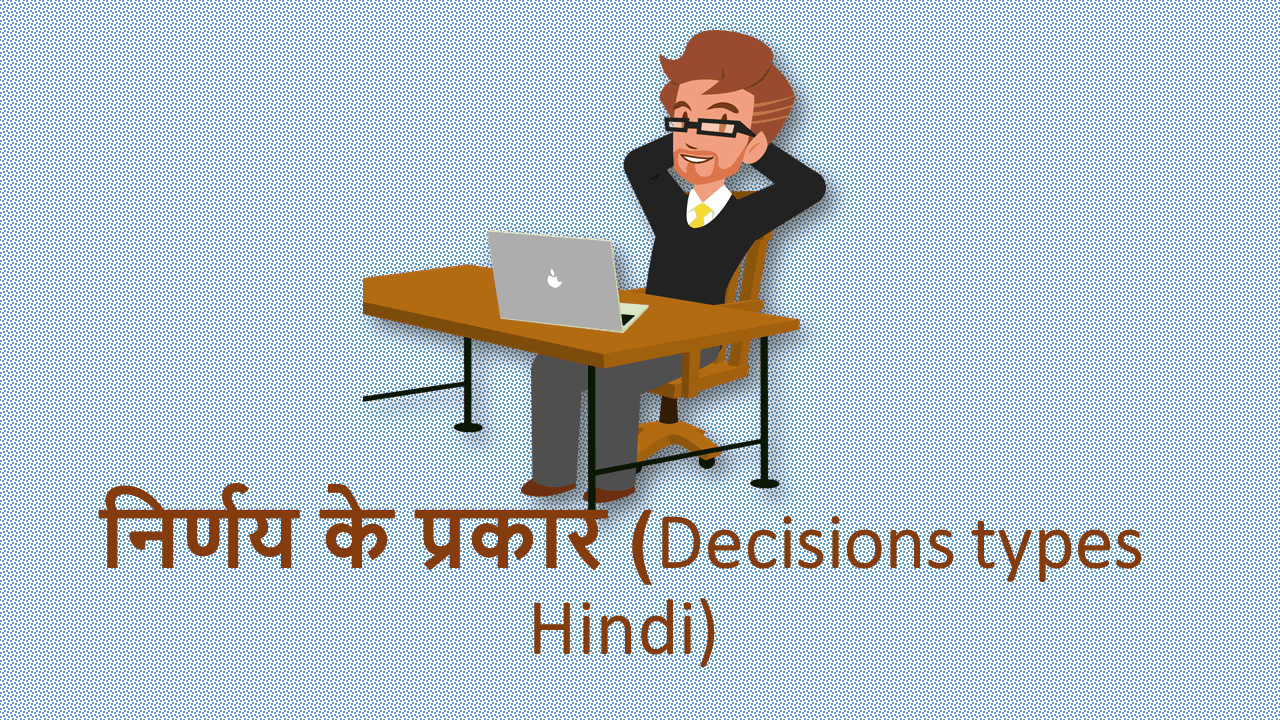प्रतिनिधिमंडल और विकेंद्रीकरण: वे निकट से संबंधित अवधारणाएं हैं; विकेंद्रीकरण प्रतिनिधिमंडल का एक विस्तार है। यह प्रतिनिधिमंडल की तुलना में व्यापक और परिणामी है; Szilagyi लिखते हैं, “केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण को दो अलग-अलग अवधारणाओं के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन प्रतिनिधिमंडल के एक निरंतरता के विपरीत छोर।” प्रतिनिधिमंडल और विकेंद्रीकरण के बीच प्राथमिक अंतर, यह अंग्रेजी में भी पढ़ो और सीखो: प्रतिनिधिमंडल दूसरों को अधिकार सौंपने की प्रक्रिया है; संगठनों के भीतर उच्च से निचले स्तर तक शक्ति को प्रत्यायोजित करने की इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप विकेंद्रीकरण होता है; इस प्रकार प्रतिनिधिमंडल विकेंद्रीकरण को प्रभावित करने के साधन के रूप में समझ सकता है।
संगठन कार्य में प्रतिनिधिमंडल और विकेंद्रीकरण के बीच अंतर क्या है?
एक संगठन में, सभी कार्यों को पूरी तरह से करना और सभी निर्णय लेना संभव नहीं है। इसके कारण उनका अधिकार अस्तित्व में आया; आम तौर पर, दोनों के अर्थों के बारे में कुछ भ्रम है क्योंकि इस तथ्य के कारण दोनों के संबंध में प्रक्रिया लगभग समान है।
कुछ लोग उन्हें पर्यायवाची मानते हैं लेकिन यह गलत है; उनका अंतर एक उदाहरण की मदद से समझ सकता है; मान लीजिए, एक महाप्रबंधक उत्पादन विभाग के प्रबंधक को अपने विभाग में $ 500 से कम के वेतन श्रेणी वाले कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है, तो यह प्रतिनिधिमंडल को बुलाएगा।
इसके विपरीत, यदि कर्मचारियों को नियुक्त करने का यह अधिकार सभी विभागों के प्रबंधकों को दिया जाता है, तो यह विकेंद्रीकरण कहलाएगा; यदि विभागीय प्रबंधक इस अधिकार को अपने विभाग के उप-प्रबंधक को सौंपता है, तो यह विकेंद्रीकरण का विस्तार होगा; इस संदर्भ में, यह कहा जाता है कि यदि हम प्राधिकरण को सौंपते हैं, तो हम इसे दो से गुणा करते हैं, यदि हम इसे विकेंद्रीकृत करते हैं, तो हम इसे कई से गुणा करते हैं।
प्रतिनिधिमंडल और विकेंद्रीकरण का अर्थ:
प्रतिनिधिमंडल का अर्थ है एक व्यक्ति द्वारा प्राधिकारी का पास होना जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए बेहतर स्थिति में है जो उसके अधीनस्थ है; यह प्राधिकरण का अधूरा कार्य है, जिससे प्रबंधक अधीनस्थों के बीच काम का आवंटन करता है; दूसरी ओर, विकेंद्रीकरण से तात्पर्य शीर्ष स्तर के प्रबंधन द्वारा अन्य स्तर के प्रबंधन द्वारा शक्तियों के फैलाव से है; यह कॉर्पोरेट सीढ़ी के दौरान शक्तियों और जिम्मेदारी का व्यवस्थित हस्तांतरण है; यह स्पष्ट करता है कि संगठनात्मक पदानुक्रम में निर्णय लेने की शक्ति कैसे वितरित की जाती है।
प्रतिनिधिमंडल और विकेंद्रीकरण के बीच मुख्य अंतर:
नीचे दिए गए प्रतिनिधिमंडल और विकेंद्रीकरण के बीच निम्नलिखित मुख्य अंतर हैं;
1] अर्थ:
प्रतिनिधिमंडल का अर्थ है कि प्रबंधक अपने कुछ कार्य और अधिकार अपने अधीनस्थों को सौंपते हैं; दूसरी ओर विकेंद्रीकरण का मतलब है, निर्णय लेने का अधिकार शीर्ष प्रबंधन और प्रबंधन के अन्य स्तरों द्वारा साझा किया जाता है।
2] प्रकृति:
प्रतिनिधिमंडल प्रबंधन की अवधि के लिए मानव सीमा का परिणाम है, यह एक नियमित कार्य है; विकेंद्रीकरण में दूसरी ओर, उद्यम के बड़े आकार और विविध कार्यों का परिणाम है, और उद्यम का एक महत्वपूर्ण निर्णय भी है।
3] ज़िम्मेदारी:
प्रतिनिधिमंडल में, बेहतर प्रतिनिधि किसी अधीनस्थ के कुछ अधिकारों और कर्तव्यों को स्थानांतरित करता है; लेकिन, उस काम के संबंध में उसकी जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती है; प्रबंधकों की जिम्मेदारी बनी रहती है और उन्हें प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है; दूसरी ओर, विकेंद्रीकरण उसे जिम्मेदारी से मुक्त करता है और अधीनस्थ उस कार्य के लिए उत्तरदायी हो जाता है; साथ ही साथ अधीनस्थों को जिम्मेदारी भी सौंपी जाती है।
4] प्रक्रिया:
प्रतिनिधिमंडल प्रसंस्करण है, जो बेहतर अधीनस्थ संबंध को स्पष्ट करता है; जबकि विकेंद्रीकरण प्रबंधकीय पदानुक्रम में सबसे निचले स्तर तक प्राधिकरण के प्रतिनिधिमंडल को बनाने की एक जानबूझकर नीति का परिणाम है; यह भी एक परिणाम है जो शीर्ष प्रबंधन और अन्य सभी विभागों के बीच संबंधों को बताता है।
5] आवश्यकता:
प्रबंधन को काम के लिए संगठन में काम करने के लिए प्रतिनिधि सौंपना लगभग आवश्यक है; अर्थात्, असाइन किए गए कार्य के प्रदर्शन के लिए अपेक्षित अधिकार सौंपना; संगठन में एक व्यवस्थित नीति के रूप में विकेंद्रीकरण का अभ्यास किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है।
6] नियंत्रण:
प्रतिनिधिमंडल में, संगठन की गतिविधियों पर अंतिम नियंत्रण शीर्ष कार्यकारी के साथ होता है; जबकि विकेंद्रीकरण में नियंत्रण की शक्ति इकाई प्रमुख द्वारा प्रयोग की जाती है; जिसके लिए प्राधिकरण को सौंप दिया गया है।
7] प्राधिकरण:
प्रतिनिधिमंडल प्राधिकरण के फैलाव का चयन करने का प्रतिनिधित्व करता है; जबकि विकेंद्रीकरण स्वायत्त और आत्मनिर्भर इकाइयों या डिवीजनों के निर्माण का प्रतीक है।
8] क्षेत्र:
प्रतिनिधिमंडल शायद ही प्राधिकरण के प्रतिनिधि को समन्वय की कोई समस्या पैदा करता है; साथ ही प्रतिनिधिमंडल का दायरा भी सीमित होता है क्योंकि बेहतर प्रतिनिधि व्यक्तिगत आधारों पर अधीनस्थों को शक्तियां सौंपता है; जबकि विकेंद्रीकरण इस संबंध में एक बड़ी समस्या है, क्योंकि लोगों को आत्मनिर्भर या स्वायत्त इकाइयाँ बनाकर कार्रवाई की अत्यधिक स्वतंत्रता दी जाती है; साथ ही गुंजाइश भी व्यापक होती है क्योंकि निर्णय लेने की प्रक्रिया अधीनस्थों द्वारा भी साझा की जाती है।
9] अच्छा परिणाम:
विकेंद्रीकरण केवल बड़े संगठनों में प्रभावी है; जबकि प्रतिनिधिमंडल की आवश्यकता होती है और सभी प्रकार के संगठनों में अच्छे परिणाम देते हैं, चाहे उनका आकार कुछ भी हो।
10] महत्व:
संगठन बनाने के लिए प्रतिनिधिमंडल आवश्यक है; जबकि शीर्ष प्रबंधन के विवेक पर विकेंद्रीकरण एक वैकल्पिक नीति है।